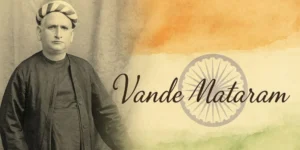वेद में सन्निहित ज्ञान विज्ञान आज भी प्रासंगिक — पुरी शंकराचार्य
भुवन वर्मा बिलासपुर 6 अगस्त 2020

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
जगन्नाथपुरी — ऋग्वेदीय पूर्वाम्नाय श्रीगोवर्धनमठ पुरीपीठाधीश्वर अनन्तश्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुरू शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वती जी महाभाग ने श्रीगोवर्धनमठ पुरी में आयोजित संगोष्ठी में कहा कि वेद में सन्निहित ज्ञानविज्ञान आज इस राकेट, कम्यूटर , मोबाईल, ऐटमबम के युग में भी प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि इस सर्ग में एक अरब सन्तानबे करोड़ उन्तीस लाख उन्चास हजार एक सौ बीस (1,97,29,49,120) वर्षों की हमारी सनातनी परम्परा है ,सकल ज्ञान — विज्ञान का स्रोत सनातन शास्त्र ही है । इन सनातन शास्त्रों में उपलब्ध ज्ञान — विज्ञान हर काल , हर परिस्थिति में हर के लिये उपयोगी है। प्रकृति में जो भी पदार्थ परिलक्षित होती है , उसके पीछे भगवान की शक्ति है। समस्त पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है ,ऊर्जा का परिवर्तित रूप आत्मा है , आत्मा परमात्मा का ही अंश है , अतः परमात्मा ही सम्पूर्ण ऊर्जा का स्त्रोत है। हमारे परमात्मा की विशेषता है कि वह जगत बनता भी है और जगत बनाता भी है । परमात्मा की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। वेद में वर्णित तथ्य के अनुसार ज्ञान विज्ञान का सम्मिलित रूप ही विद्या है। किसी पदार्थ या वस्तु के संबंध में सामान्य बोध का नाम ज्ञान है , वहीं उस पदार्थ या वस्तु के संबंध में विशेष बोध का नाम विज्ञान है। वैज्ञानिक वह होता है जो सामान्य वस्तु को विशेष का रूप प्रदान करने में समर्थ होता है , ठीक इसी प्रकार विशेष वस्तु को सामान्य में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। प्रकृति में प्रमुख पांच तत्त्व पृथ्वी , जल , तेज , वायु और आकाश है। पृथ्वी , जल , तेज , वायु , आकाश , प्रकृति , परमात्मा आदि ही विज्ञान के स्त्रोत हैं , इन सभी में सन्निहित गुण या सूक्ष्म ज्ञान को समझना , प्राप्त करना या उजागर करना ही विज्ञानदृष्टि है। प्रकृति के स्वरूप को समझने से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। प्रत्येक प्राणी की चाह मृत्यु के भय से मुक्त होकर अमरत्व की होती है , अनेक उदाहरणों से स्पष्ट है कि जिस वस्तु की चाह होती है उसका अस्तित्व अवश्य होता है । उदाहरण के लिये भूख का लगना अन्न के अस्तित्व को सिद्ध करता है , जहां प्यास होगी वहां पूर्ति के लिये जल अवश्य होगा । तात्पर्य यह निकला कि यदि हमारी चाह का विषय अंश के रूप में मृत्युंजय सच्चिदानन्द स्वरूप सर्वेश्वर हैंजोकि अंशी हैं तो उनका अस्तित्व भी अवश्य होगा। अतः परमात्मा ही समस्त ज्ञान विज्ञान के स्त्रोत हैं। मंत्र , तंत्र , यंत्र को परिभाषित करते हुये पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा कि उत्तम वैज्ञानिक वह होता है जो पंच तत्व ( पृथ्वी , जल , तेज , वायु और आकाश ) में सन्निहित सूक्ष्म सिद्धांत को आत्मसात कर सके , यही मंत्रसिद्धि होता है , इस सूक्ष्म ज्ञान को यंत्र के रूप में परिवर्तित कर लोकोपयोगी बनाना तंत्र है। यंत्र द्वारा लोकोपयोगी कार्य का क्रियान्वयन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से ही प्रकृति सुरक्षित रह सकती है।पूज्यपाद पुरी शंकराचार्य जी ने बताया कि विभिन्न शास्त्रों में उल्लेखित तथ्य के अनुसार किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं हो सकती और आकस्मिक नाश भी नहीं होता , इसका तात्पर्य अव्यक्त पदार्थ को व्यक्त के रूप में परिवर्तित करते हैं। किसी पदार्थ के नाश का अर्थ व्यक्त को अव्यक्त के रूप में परिवर्तन करना है , यही उसका मौलिक स्वरुप है। हमारा यह स्थूल शरीर एक यंत्र की तरह है जिसके संचालन के लिये सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। बिना सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति में हमारा यह स्थूल शरीर शव हो जाता है। सृष्टि की संरचना में पांच तत्वों की भूमिका है, पृथ्वी , जल , तेज , वायु और आकाश । मिट्टी के विशिष्ट गुण गंध का कर्षण करने पर वह जल में परिवर्तित हो जाता है अर्थात जिस वस्तु में जो नैसर्गिक गुण होता है उसका कर्षण करने पर वह कारण में बदल जाता है । ठीक इसी प्रकार जल के निसर्गसिद्ध गुण रस के कर्षण से वह अपने कारण तेज में , तेज के विशिष्ट गुण रूप के कर्षण से वह अपने कारण वायु मे तथा वायु के नैसर्गिक गुण स्पर्श के कर्षण से वह आकाश में परिवर्तित हो जाता है । इस गूढ़ रहस्य को समझना एवं प्राप्त करना ही वैज्ञानिक कार्य है। हमारे जीवन के प्रत्येक गतिविधि में दर्शन एवं विज्ञान घुला हुआ है। पुरी शंकराचार्य जी आगे महायंत्रो की चर्चा करते हुये कहा कि आधुनिक युग में महायंत्रो के उपयोग का प्रयोजन समय की , श्रम की , सहयोगियों की , सामग्रियों की बचत के लिये किया जाता है तथा इस बचत का उपयोग वह मौज-मस्ती पूर्ण जीवन में करना चाहता है। परंतु महायंत्रो के उपयोग के बाद भी समय की कमी , सहयोगी की कमी , सामग्री की कमी होना इसके निर्माण के प्रयोजन को ही विफल कर देता है। मानव जीवन का वास्तविक ध्येय स्वयं को कृतार्थ करना है , परंतु इसके लिये धैर्य , संयम और समय ही नहीं है। हर व्यक्ति आधुनिक विकासपरक व यांत्रिक युग में तनाव ग्रस्त है , जो महायंत्रो के प्रयोजन को विफल करता है। शास्त्र के अनुसार गंतव्य का ज्ञान होने पर ही गन्ता लक्ष्य की ओर पहुंँच सकता है , विज्ञान के लक्ष्य का निर्धारण नहीं है , इसीलिये वह प्रकृति की रक्षा करने में असफल है । इसके लिये सृष्टि संरचना का उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिये। महाप्रलय के पश्चात परमात्मा द्वारा पुनः सृष्टि रचना का उद्देश्य अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ करने का अवसर प्रदान करना है जिससे कि वह पंचभूत पृथ्वी , जल , तेज , वायु, आकाश और प्रकृति का आलम्बन लेकर कृतार्थ हो सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। सृष्टि संरचना के उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिये तभी विज्ञान को सही दिशा मिल सकती है। देहात्मवादी भौतिक शरीर को ही सबकुछ मानते हैं , परंतु गाढी़ नींद उनके सिद्धांत पर पानी फेरता है क्योंकि यदि भौतिक शरीर का ऐच्छिक सुख अर्थात प्रिय ( चाही गई वस्तु की प्राप्ति ), मोद ( चाही गई वस्तु से पूर्ण संतुष्टि ) और प्रमोद (अधिकतम संतुष्टि ) को त्यागकर जो कि विषयजन्य आनंद है , नींद की अपेक्षा रखता है , बिना नींद के विक्षिप्तता को प्राप्त कर लेगा। निष्कर्ष यह निकला कि जीवन में सिर्फ विषयजन्य आनंद ही सब कुछ नहीं है । जीव जगत का आलम्बन लेकर ही जीवनधन जगदीश्वर की प्राप्ति कर सकता है जो कि धैर्य एवं संयम के बिना संभव नहीं। महायंत्रो के प्रचुर आविष्कार एवं प्रयोग से हमारा जीवन ना तो भोग के अनुकूल और ना ही मोक्ष के अनुकूल रह गया है। महायंत्रो के प्रचुरता से आर्थिक विषमता एवं विपन्नता उत्पन्न हो रही है। सृष्टि के आवश्यक तत्व पृथ्वी , जल , तेज , वायु मलीन, कुपित हो रहे हैं जोकि महामारी , विश्व युद्ध , विभिन्न प्रजातियों के लोप का कारण है।
About The Author